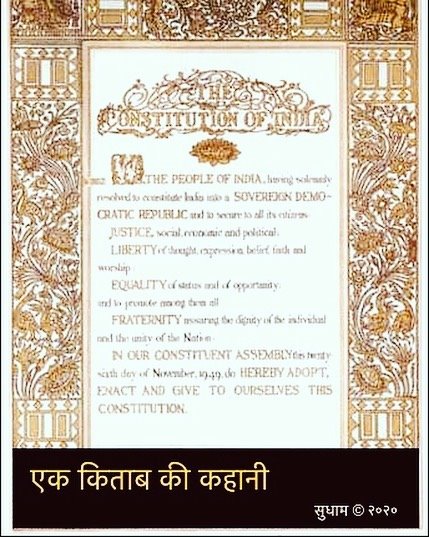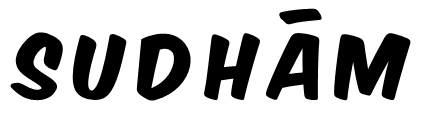क्या बेवजह बढ़ रहें हैं ये क़ाफ़िले
कौन सी है वो मंज़िल चल पड़े जिस रास्ते
कुछ तो होगा मसला-ए-जुनून
छिड़ गया है इंक़लाब जिस के वास्ते
कितना और रुकें के जब होगी वो सुबह
छीनी आज़ादी जिस लिए फ़िरंगी हाथ से
रंजिशें तो तब भी उबल के उभरी थीं
क़ीमत तो चुकायी लेकिन क्या सीखा सरहदें बाँट के
सिकती रही है बिकती भी रहेगी सियासी रोटी
थकते नहीं ये ले ले कर भूखे मज़्लूमों के नाम
बनती भी हैं और गिराई भी जाती हैं सरकारें
आज़माती है हक़-ए-जम्हूरियत जब अवाम
हर कोई कहे मैं सही हूँ और वो ग़लत
फ़िर दूर दूर खड़े हैं लोग आईन लिए हाथ में
देर आयेगी पर समझ आयेगी ये बात यक़ीनन
पन्ने बस अलहदा हैं लेकिन हैं उसी किताब के